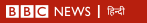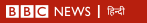अगले दो हफ़्तों तक जलवायु सम्मेलन COP28 की चर्चा खूब सुनाई देने वाली है। जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया की सबसे अहम बैठक गुरुवार से दुबई में हो रही है, जिसकी मेज़बानी दुनिया के शीर्ष 10 तेल उत्पादक देशों में एक संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) कर रहा है।
COP28 दुनिया भर के शीर्ष नेताओं का इस साल का सबसे बड़ा जुटान है और इसमें 70,000 के क़रीब और लोग शामिल होंगे।
पेट्रोल उत्पादक देश में जलवायु सम्मेलन आयोजित किया जाना पहले से ही विवादों में था, लेकिन बीबीसी को मिले साक्ष्यों से पता चलता है कि यूएई टीम ने COP28 जलवायु सम्मेलन से पहले तेल और गैस के सौदे की योजना बना रखी है, जिसने चिंता को और बढ़ा दिया है।
तो क्या तेल उत्पादन में दुनिया के सबसे धनी देश में हो रहे सम्मेलन से जलवायु परिवर्तन को लेकर कोई सार्थक एक्शन निकल सकता है?
पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने कहा है कि ये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बस ‘यूं ही हैं’- यानी इसमें बातें तो बहुत होती हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन अगर COP प्रक्रिया का अस्तित्व नहीं होता, तो हम इस तरह की कोई ढांचा ज़रूरत चाहते।
पहले के समझौते
कल्पना करिए कि आप धरती पर भ्रमण करने वाला कोई एलियन हैं। और आपको पता चलता है कि यहां रहने वालों की गतिविधियों से ही इस ग्रह को संभावित महाविनाश का ख़तरा पैदा हो गया है।
तो पहली बात जो एलियन कहेगा, वो ये है, “आप सभी को एक साथ बैठने और इसे हल करने पर राज़ी होने की ज़रूरत है।”
लेकिन इस दिशा में प्रगति करना कठिन है।
आपको इस बात पर ताज्जुब हो सकता है कि जब पहली बार दुनिया सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कटौती करने पर सहमत हुई थी, जो कि जलवायु परिवर्तन का कारण है, वो आठ साल पहले पेरिस में हुए COP21 सम्मेलन में हुआ था।
क़रीब 200 देशों ने वैश्विक तापमान वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने और इसे 1।5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का संकल्प लिया था।
संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिकों का मानना है कि सबसे ख़तरनाक पर्यावरणीय प्रभावों से बचने के लिए यह ज़रूरी है।
संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि साल 2015 में हुआ वो पेरिस समझौता एक बड़ा क़दम था और इसने ‘लगभग वैश्विक जलवायु कार्रवाई’ को गति दी। इससे दुनिया में अपेक्षित तपमान वृद्धि के स्तर को कम करने में मदद मिली।
संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि, लेकिन पेरिस में तय किए गए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अभी भी दुनिया उस गति से एक्शन नहीं ले रही है। मौजूदा सम्मेलन में इसे हल करने की कोशिश, एक बड़ा मुद्दा होगा।
COP28 जलवायु सम्मेलन में क्या होगा?
इस सम्मेलन में सबसे ऊपर एजेंडा होगा कि सरकारों से कार्यवाही के वादे करने पर और व्यापक सहमति लेने की कोशिश की जाए। इसे संयुक्त राष्ट्र की शब्दावली में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान या एनडीसी कहा जाता है।
इसके पीछे विचार ये है कि किए गए वायदे समय के साथ और कड़े हों और लक्ष्यों को लगातार बढ़ाया जाए।
COP28 में एक ऐसा समझौता कराने की उम्मीद है, जिसमें एनडीसी को और व्यापक बनाया जाना चाहिए जो फूड और खेती समेत सभी आर्थिक गतिविधियों में होने वाले उत्सर्जन को कवर करे।
इसके अलावा ये भी कोशिश होगी कि देशों को उनके किए वायदों के लिए और अधिक जवाबदेह बनाया जाए जो कि एक लंबी प्रक्रिया है।
इस समय, संयुक्त राष्ट्र प्रक्रिया के तहत पेरिस समझौता देशों पर कुछ भी करने के लिए दबाव नहीं डाल सकता। सभी एक्शन स्वैच्छिक हैं।
एक और मुद्दा होगा फ़ंड का। इस बात पर बहुत चर्चा होगी कि किस काम के लिए कौन फ़ंड देगा।
जलवायु सम्मेलन में ग़ैर बराबरी का मुद्दा
अच्छी ख़बर है कि वायु और सौर ऊर्जा की रेन्यूएबल टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती हुई है और बहुत सारे मामलों में इनसे पैदा होने वाली बिजली जीवाश्म ईंधन के मुकाबले अब कम खर्चीली है।
यूएई का एक लक्ष्य है, साल 2030 तक दुनिया की अक्षय ऊर्जा क्षमता को तिगुना करने पर दुनिया को सहमत कराना, जिस पर अमेरिका, चीन और अन्य जी20 देश पहले से सहमत हैं। वो 2030 तक ऊर्जा दक्षता सुधार की दर को दोगुना करने पर भी सहमति पैदा करना चाहता है।
इन उपायों के लिए बहुत बड़े निवेश की ज़रूरत होती है, भले ही बाद में ये बचत दे सकें।
हमें पहले से पता है कि जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने और इसकी तैयारी करने में ख़रबों डॉलर का खर्च होना है।
इन चर्चाओं के केंद्र में गहरी ग़ैर-बरारी भी है जो दुनिया को बाँटती है। सबसे अधिक धनी देश जीवाश्म ईंधन के बूते ही धनी बने।
ग़रीब देशों का कहना है कि अमीर देशों को अब उस धन का इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए उन्हें मदद करने में करना चाहिए क्योंकि अमीर दुनिया ने इसे पैदा किया है।
विकसित देशों द्वारा जलवायु एक्शन के लिए विकासशील देशों को हर साल 100 अरब डॉलर की मदद का वादा किया गया था। शुरू में ये वादा 2020 तक का था, लेकिन लगता है कि ये आख़िरकार अब पूरा हो गया है।
ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान नकदी प्रवाह में मदद के लिए कर्ज़ देने के अपने नियमों को बदलने के दबाव के आगे झुक रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है।
'फ़ेज डाउन' या 'फ़ेज आउट'?
साल 2022 में मिस्र में हुए COP27 की सबसे बड़ी सफलता थी, जलवायु परिवर्तन से आने वाली आपदाओं में सबसे ग़रीब देशों को मदद के लिए एक नया ‘लॉस एंड डैमेज’ फ़ंड स्थापित करने पर सहमति बनाना।
लेकिन वो कौन से देश हैं जो इस फ़ंड में योगदान करेंगे? यूरोपीय संघ ने संकेत दिया है कि वो अपना खजाना खोलने जा रहा है, लेकिन अमेरिका और अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का क्या?
चीन, सऊदी अरब और खाड़ी के देश COP उद्देश्यों के लिए अभी भी विकासशील देशों के रूप में दर्ज हैं और इसलिए इस तरह के फ़ंड में योगदान देने के लिए मजबूर नहीं हैं- जोकि विवाद का एक बड़ा कारण है।
और अंततः हम उसी पुराने COP मुद्दे की लौटने की उम्मीद कर सकते हैं- यानी ‘धीरे धीरे कम करना या बिल्कुल बंद करने’ का खेल।
असल में यह एक परिभाषा है जो कोयला, तेल और गैस जैसे निर्बाध जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को लेकर दुनिया की दीर्घकालिक महत्वाकांक्षा के लिए किया जाता है।
दूसरे शब्दों में, क्या दुनिया को समय के साथ प्रदूषण पैदा कनरे वाले जीवाश्म ईंधन के उत्पादन और इस्तेमाल में धीरे धीरे कमी लानी चाहिए (’फ़ेज डाउन’) या इस पर पूरी तरह प्रतिबंध की तारीख़ तय करनी चाहिए (’फ़ेज आउट’)- लेकिन ये कब किया जाना चाहिए?
इस साल का यह सबसे उपयुक्त सवाल है, क्योंकि यह सम्मलेन उस तेल उत्पादक देश में हो रहा है जो अपनी तेल उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना बना रहा है।
COP28 के अध्यक्ष सुल्तान अल-जाबेर ‘फ़ेज़ डाउन’ चाहते हैं लेकिन लगता कि यूरोपीय संघ समेत कई देश पूरी तरह ‘फ़ेज़ आउट’ के लिए जोर लगाएंगे।
ये ताज्जुब लग सकता है कि दुनिया ने अभी भी इन दोनों में से किसी पर भी आधिकारिक प्रतिबद्धता ज़ाहिर नहीं की है।
और यह चेतावनियों के बावजूद है कि दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग को 1।5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए जितना ज़रूरी है उसके मुकाबले, जीवाश्म ईंधन का मौजूदा और निकट भविष्य में होने वाला उत्पादन पहले ही बहुत अधिक है।