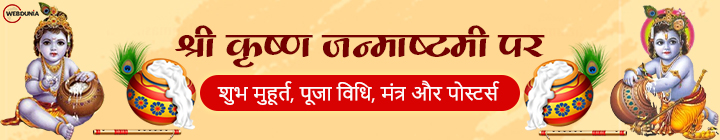-प्रभुदयाल मिश्रा
भारतीय ऋषियों ने जगत के रहस्य को 6 कोणों से समझने की कोशिश की है। वे जानते थे कि मानव की सबसे बड़ी इच्छा दु:ख से छुटकारा है। वे इसके प्रति भी आश्वस्त थे कि इन सिद्धांतों के जरिए उन्होंने इसका निदान खोज लिया है। आइए देखें, ये दार्शनिक सिद्धांत क्या हैं और उनके प्रणेता कौन-कौन हैं--
न्याय : तर्क प्रधान इस प्रत्यक्ष विज्ञान की शुरुआत करने वाले अक्षपाद गौतम हैं। यहाँ न्याय से मतलब उस प्रक्रिया से है जिससे मनुष्य किसी नतीजे पर पहुँच सके - नीयते अनेन इति न्यायः।
प्रत्येक ज्ञान के लिए चार चीजों का होना आवश्यक है -
1. प्रमाता अर्थात् ज्ञान प्राप्त करने वाला। 2. प्रमेय अर्थात् जिसका ज्ञान प्राप्त करना अभीष्ट है। 3. ज्ञान और 4. प्रमाण अर्थात ज्ञान प्राप्त करने का साधन।
वैशेषिक दर्शन : महर्षि कणाद ने इस दार्शनिक मत द्वारा ऐसे धर्म की प्रतिष्ठा का ध्येय रखा है जो भौतिक जीवन को बेहतर बनाए और लोकोत्तर जीवन में मोक्ष का साधन हो।
'यतोम्युदय निश्रेयस सिद्धि: स धर्मः'
न्याय दर्शन जहाँ अंतर्जगत और ज्ञान की मीमांसा को प्रधानता देता है, वहीं वैशेषिक दर्शन बाह्य जगत की विस्तृत समीक्षा करता है। इसमें आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए इसे अजर, अमर और अविकारी माना गया है।
न्याय और वैशेषिक दोनों ही दर्शन परमाणु से संसार की शुरुआत मानते हैं। इनके अनुसार सृष्टि रचना में परमाणु उपादान कारण और ईश्वर निमित्त कारण है। इसके अनुसार जीवात्मा विभु और नित्य है तथा दुःखों का खत्म होना ही मोक्ष है।
समस्त वस्तुओं को कुल सात पदार्थों के अंतर्गत माना गया है -
1. द्रव्य, 2. गुण, 3. कर्म, 4. सामान्य, 5. विशेष, 6. समवाय, 7. अभाव।
मीमांसा : वेद के मुख्य दो भाग हैं - कर्मकांड और वेदांत। संहिता और ब्राह्मण में कर्मकांड का प्रतिपादन किया गया है तथा उपनिषद् एवं आरण्यक में ज्ञान का। मीमांसा दर्शन के आद्याचार्य जैमिनी ने इस कर्मकाण्ड को सिद्धांतबद्ध किया है।
इस दार्शनिक मत के अनुसार प्रतिपादित कर्मों द्वारा ही मनुष्य अभीष्ट प्राप्त कर सकता है। इसके अनुसार कर्म तीन प्रकार के हैं - काम्य, निषिद्ध और नित्य। वास्तव में बिना कर्म के ईश्वर भी फल देने में समर्थ नहीं है।
मीमांसा दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हुए बहुदेववादी है। इसमें यज्ञादि कर्मों के परिणाम के लिए एक अदृश्य शक्ति की कल्पना की गई है, जो मनुष्य को शुभ और अशुभ फल देती है।
सांख्य : सच पूछा जाए तो यह एक द्वैतवादी दर्शन है। इसके अनुसार विश्व प्रपंच के प्रकृति और पुरुष दो मूल तत्व हैं। पुरुष चेतन तत्व है और प्रकृति जड़। इसके अनुसार जगत का उपादान तत्व प्रकृति है। सत्व, रज और तम आदि तीन गुण इसके अभिन्न अंग हैं। जब इन तीनों गुणों की साम्यावस्था भंग हो जाती है और उसके गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता है तब सृष्टि का आरंभ होता है।
वेदांत : महर्षि वादरायण जो संभवतः वेदव्यास ही हैं, का 'ब्रह्मसूत्र' और उपनिषद वेदांत दर्शन के मूल स्रोत हैं। आदि शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और श्रीमद्भगवद् गीता पर भाष्य लिखकर अद्वैत मत का जो प्रतिपादन किया उसका भारतीय दर्शन के विकास में इतना प्रभाव पड़ा है कि इन ग्रन्थों को ही 'प्रस्थान त्रयी' के नाम से जाना जाने लगा। वेदांत दर्शन निर्विकल्प, निरुपाधि और निर्विकार ब्रह्म को ही सत्य मानता है।
'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' इसके अनुसार जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से ही होती है - 'जन्माद्यस्य यतः' (ब्रह्म सूत्र - 2), उत्पन्न होने के पश्चात जगत ब्रह्म में ही मौजूद रहता है और आखिरकार उसी में लीन हो जाता है। इसके अनुसार जगत की यथार्थ सत्ता नहीं है। सत्य रूप ब्रह्म के प्रतिबिम्ब के कारण ही जगत सत्य प्रतीत होता है।
जीवात्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं है। अविधा से आच्छादित होने पर ही ब्रह्म जीवात्मा बनता है और अविधा का नाश होने पर वह उसमें तद्रूप होता है।
योग : महर्षि पतंजलि का 'योगसूत्र' योग दर्शन का प्रथम व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है। योगदर्शन इन चार विस्तृत भाग, जिन्हें इस ग्रंथ में पाद कहा गया है, में विभाजित है- समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद तथा कैवल्यपाद। प्रथम पाद का मुख्य विषय चित्त की विभिन्न वृत्तियों के नियमन से समाधि द्वारा आत्म साक्षात्कार करना है।
द्वितीय पाद में पाँच बहिरंग साधन - यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का विवेचन है। तृतीय पाद में अंतरंग तीन धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन है। इसमें योगाभ्यास के दौरान प्राप्त होने वाली विभिन्न सिद्धियों का भी उल्लेख हुआ है, किन्तु ऋषि के अनुसार वे समाधि के मार्ग की बाधाएँ ही हैं। चतुर्थ कैवल्यपाद मुक्ति की वह परमोच्च अवस्था है, जहाँ एक योग साधक अपने मूल स्रोत से एकाकार हो जाता है।
दूसरे ही सूत्र में योग की परिभाषा देते हुए पतंजलि कहते हैं - 'योगाश्चित्त वृत्तिनिरोधः'। अर्थात योग चित्त की वृत्तियों का संयमन है। चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए महर्षि पतंजलि ने द्वितीय और तृतीय पाद में जिस अष्टांग योग साधन का उपदेश दिया है, उसका संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है :-
1. यम : कायिक, वाचिक तथा मानसिक इस संयम के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय चोरी न करना, ब्रह्मचर्य जैसे अपरिग्रह आदि पाँच आचार विहित हैं। इनका पालन न करने से व्यक्ति का जीवन और समाज दोनों ही दुष्प्रभावित होते हैं।
2. नियम : मनुष्य को कर्तव्य परायण बनाने तथा जीवन को सुव्यवस्थित करते हेतु नियमों का विधान किया गया है। इनके अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान का समावेश है। शौच में बाह्य तथा आन्तर दोनों ही प्रकार की शुद्धि समाविष्ट है।
3. आसन : पतंजलि ने स्थिर तथा सुखपूर्वक बैठने की क्रिया को आसन कहा है। परवर्ती विचारकों ने अनेक आसनों की कल्पना की है। वास्तव में आसन हठयोग का एक मुख्य विषय ही है। इनसे संबंधित 'हठयोग प्रतीपिका' 'घरेण्ड संहिता' तथा 'योगाशिखोपनिषद्' में विस्तार से वर्णन मिलता है।
4. प्राणायाम : योग की यथेष्ट भूमिका के लिए नाड़ी साधन और उनके जागरण के लिए किया जाने वाला श्वास और प्रश्वास का नियमन प्राणायाम है। प्राणायाम मन की चंचलता और विक्षुब्धता पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत सहायक है।
5. प्रत्याहार : इंद्रियों को विषयों से हटाने का नाम ही प्रत्याहार है। इंद्रियाँ मनुष्य को बाह्यभिमुख किया करती हैं। प्रत्याहार के इस अभ्यास से साधक योग के लिए परम आवश्यक अन्तर्मुखिता की स्थिति प्राप्त करता है।
6. धारणा : चित्त को एक स्थान विशेष पर केंद्रित करना ही धारणा है।
7. ध्यान : जब ध्येय वस्तु का चिंतन करते हुए चित्त तद्रूप हो जाता है तो उसे ध्यान कहते हैं। पूर्ण ध्यान की स्थिति में किसी अन्य वस्तु का ज्ञान अथवा उसकी स्मृति चित्त में प्रविष्ट नहीं होती।
8. समाधि : यह चित्त की अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। योग दर्शन समाधि द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति को संभव मानता है।
समाधि की भी दो श्रेणियाँ हैं - सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात। सम्प्रज्ञात समाधि वितर्क, विचार, आनंद और अस्मितानुगत होती है। असम्प्रज्ञात में सात्विक, राजस और तामस सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है।