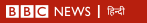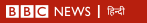मई 2022। दुनिया भर की नज़र स्विट्ज़रलैंड के दावोस पर टिकी थीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम में आला कारोबारी और नेता जुटे थे। वहां दुनिया के सामने मौजूद सबसे बड़े संकट का समाधान तलाशने पर चर्चा होनी थी।
इसके तीन महीने पहले जब दुनिया भर के खाद्य बाज़ार बढ़ती कीमतों समेत कई झटके झेल रहे थे तभी रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेन से दूसरे देशों को कई टन अनाज भेजा जाना था लेकिन युद्ध की वजह से अहम रास्ते बंद हो गए और सप्लाई नहीं हो सकी।
संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के प्रमुख डेविड बीज़ली भी दावोस में थे। उन्होंने आगाह किया कि मुश्किल से उबरने का वक़्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। दुनिया बड़े खाद्य संकट का सामना कर रही है और आगे स्थिति कहीं ज़्यादा ख़राब हो सकती है।
इसके बाद सवाल उठा कि क्या यूक्रेन-रूस युद्ध ही दुनिया के खाद्य संकट की वजह है ? इसका जवाब तलाशने के लिए बीबीसी ने चार एक्सपर्ट से बात की।
युद्ध का असर
संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुख्य अर्थशास्त्री आरिफ़ हुसैन कहते हैं, "हर कोई ब्रेड खाता है। हर कोई मक्का खाता है। हर किसी को खाने के तेल की ज़रुरत होती है। युद्ध की वजह से बने अवरोध के कारण दुनिया भर के लोग रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान हासिल नहीं कर पा रहे हैं।"
आरिफ़ हुसैन बताते हैं कि यूक्रेन की अहमियत दुनिया की 'फूड बास्केट' जैसी है। खासकर यूरोप के लिए। यूक्रेन की आबादी चार करोड़ के करीब है लेकिन वो 40 करोड़ लोगों के लिए अनाज उगाते हैं। देश की ज़रूरत पूरी करने के बाद बचा सारा अनाज बाहर जाता है।
अनुमान है कि युद्ध शुरू होने के बाद ढाई करोड़ टन से ज़्यादा अनाज ओडेसा बंदरगाह के करीब फंसा हुआ है। अगर अब जहाज़ रवाना हो भी जाते हैं तो उन्हें ब्लैक सी पार करना होगा, जहां 'फ्लोटिंग माइन्स' के रूप में एक नया ख़तरा मौजूद है।
आरिफ़ हुसैन कहते हैं कि व्यावसायिक जहाज़ वहां आने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। इस इलाके से सामान ले जाने के लिए समुद्री रास्ता ही सबसे प्रभावी है।
आरिफ़ हुसैन बताते हैं, "दूसरे विकल्प सुगम नहीं हैं। उनमें लागत बहुत बढ़ जाती है। रेल या ट्रक से सामान भेजने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि इसके लिए कितने ईंधन की ज़रूरत होगी। कितनी ट्रेन की ज़रूरत होगी। इसमें और ज़्यादा खर्च आएगा। अगर वो ऐसा करने के बारे में सोचें तो भी ये नामुमकिन होगा।"
आरिफ़ हुसैन कहते हैं कि अलग-अलग देशों में पटरियों के साइज़ अलग-अलग हैं। ऐसे में यूक्रेन की ट्रेन बिना बदलाव किए पोलैंड की पटरियों पर नहीं दौड़ पाएगी।
आरिफ़ हुसैन कहते हैं कि यूक्रेन से समुद्री रास्ते के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा 20 प्रतिशत अनाज भेजा जा सकता है लेकिन दुनिया में खाने के सामान की बढ़ती कीमतों पर रोक के लिए इतना काफ़ी नहीं है। संकट खाद को लेकर भी है।
वो कहते हैं, " यूक्रेन युद्ध के पहले भी खाद के दाम बढ़ रहे थे। युद्ध शुरू होने पर कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ीं। अगर आप पिछले साल से तुलना करें तो दाम 200 फीसदी बढ़ चुके हैं। खाद बनाने के लिए आपको गैस की ज़रूरत होती है। गैस की कीमत भी आसमान पर है। इसके मायने ये हैं कि पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन नहीं हो पाएगा और सोचिए तब क्या स्थिति होगी?"
यूक्रेन में अगली फसल का मौसम कुछ ही हफ़्ते दूर है। इसे रखने की जगह चाहिए। वहां भंडार पहले ही भरे हुए हैं। समस्याएं और भी हैं।
आरिफ़ हुसैन कहते हैं, "आप चाहे फसल लगा रहे हों या फिर फसल काट रहे हों, आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आपको लोगों की ज़रूरत होती है। किसानों की ज़रूरत होती है। अभी किसान कहां हैं? किसान सैनिक बन गए हैं। मशीनरी युद्ध में लगे लोगों की मदद के लिए तैनात है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आप अपनी फसल का ध्यान रख पाए तो आपके पास लोग नहीं होंगे और ये मत भूलिए कि युद्ध के समय खुले आसमान के नीचे खेत में बैठना आसान नहीं होता।"
आरिफ़ हुसैन का संगठन 'वर्ल्ड फूड प्रोग्राम' मुश्किल हालात का सामना कर रहा है। इसका असर खाद्य संकट से निपटने की कोशिशों पर हो सकता है।
कई देशों के कुल 15 करोड़ लोगों को खाने का सामान मुहैया कराने के लिए 22 अरब डॉलर की ज़रूरत है। संगठन अभी तक इसकी आधी रकम ही जुटा पाया है। उधर, बंदरगाह दोबारा शुरू करने को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत में कोई प्रगति नहीं दिखती।
उपजाऊ ज़मीन
'फूड सिस्टम फ़ॉर द फ्यूचर' की सीईओ अर्थरिन कज़िन बताती हैं, " यूक्रेन खेती के लिहाज से अहम उत्पादक इलाका है। यहां वही खूबियां हैं जो अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र, फ्रांस, रूस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। यहां उम्दा काली मिट्टी है। जिसमें बहुतायत में पोषक तत्व हैं। इससे किसानों को अच्छी उपज मिलती है।"
वो बताती हैं कि सरकार से मिलने वाली सब्सिडी और बड़े पैमाने पर हुए निवेश ने भी यूक्रेन में उत्पादन बढ़ाने में मदद की। यूक्रेन जिन देशों को अनाज भेजता है, वो उसी पर निर्भर हैं।
लेकिन अर्थरिन कज़िन कहती हैं, " ये कहना अतिश्योक्ति होगी कि पूरी दुनिया यूक्रेन पर निर्भर है। सच ये है कि कुल निर्यात में रूस और यूक्रेन की मिलाकर हिस्सेदारी 27 प्रतिशत है। लेकिन सोमालिया जैसे कुछ देश सौ प्रतिशत गेहूं यूक्रेन से ही मंगाते हैं। मिस्र और अफ़्रीका के कुछ दूसरे देश 'ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम' के तहत उनसे सीधे कारोबारी रिश्ते रखते हैं।"
यूक्रेन की सीमा पर रूस ने अपने सैनिकों को तैनात किया, उसके काफी पहले से कोरोना महामारी, लॉकडाउन और मज़दूरों की कमी ने सप्लाई सिस्टम को प्रभावित कर दिया था।
अर्थरिन कहती हैं कि तेल की कीमतें बढ़ने पर समुद्री रास्ते से सामान भेजना महंगा हो गया। कोविड-19 की वजह से उत्पादन भी प्रभावित हुआ और स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों का मुक़ाबला करने में विकासशील देशों का खजाना काफी हद तक खाली हो गया।
वो कहती हैं कि अभी दिक्कत की सबसे बड़ी वजह यूक्रेन ही दिखता है लेकिन ये समस्या का इकलौता कारण नहीं है। युद्ध शुरू होने पर लाखों टन गेहूं, मक्का और सनफ्लॉवर के बीज यूक्रेन में फंसे रह गए और ग़रीब देशों के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी हो गईं।
अर्थरिन कज़िन कहती हैं, "ये उपलब्धता से जुड़ी दिक्कत नहीं है। समस्या सामान तक पहुंच की है। तमाम देश वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। खाद की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। कमी पूरी करने के लिए स्थानीय स्तर पर जितने अनाज की ज़रूरत है, छोटे किसान उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं।"
अगर आप खरीदने की क्षमता रखते हैं तो ज़रूरत भर अनाज मौजूद है। निर्यात पर निर्भरता घटाने के लिए आपको अपनी ज़रूरत के लायक अनाज उगाने की व्यवस्था करनी होगी। यूक्रेन से अनाज आने का रास्ता बंद है। ऐसे में तमाम देशों को विकल्प तलाशने की ज़रूरत है। लेकिन अनाज के दूसरे उत्पादक देश हज़ारों मील की दूरी पर हैं, ऐसे में वहां से सामान मंगाना महंगा साबित होगा।
अर्थरिन इसका भी रास्ता बताती हैं। वो कहती हैं कि यातायात से जुड़ी दिक्कतें दूर करने के लिए इसमें ज़्यादा निवेश करना होगा। दुनिया भर के लाखों छोटे किसानों को भी मदद देनी होगी।
वो कहती हैं, "हमें ये तय करने की ज़रूरत है कि हमारे पास एक ऐसा वैश्विक बाज़ार हो जहां काराबोर होता रहे। हमें किसानों का उत्पादन बढ़ाने और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ भंडारों और शीतगृहों में निवेश करना होगा। दुनिया के सभी देशों में रिटेल नेटवर्क को भी सुचारू बनाना होगा ताकि स्थानीय स्तर पर खाने का सामान मौजूद रहे।"
वो आगाह करती हैं कि अगर इनमें से कुछ भी करने से छूट गया तो फूड सिस्टम की कमी बार-बार उजागर होती रहेगी और कीमतें उसी तरह बढ़ती रहेंगी जैसे हम अभी देख रहे हैं। दुर्भाग्य से अगर ये स्थिति बनी रही तो ग़रीब लोगों के बीच भूख की समस्या और भी बढ़ेगी।
निर्यात पर रोक
यूक्रेन युद्ध की वजह से निर्यात के लिए तैयार खाने के सामान की बड़ी खेप पर रोक लग गई और बाज़ार की अनिश्चितता कहीं ज़्यादा बढ़ गई। ऐसे में सरकारें नवर्स दिखने लगीं। कई देशों ने खाने के सामान का निर्यात कम कर दिया या फिर पूरी तरह पाबंदी लगा दी।
इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर रिसर्च फेलो और अर्थशास्त्री डेविड लैबोर्ड बताते हैं, "हाल में इंडोनेशिया ने पाम ऑयल निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी।"
डेविड कहते हैं कि करोड़ों लोगों के लिए पाम ऑयल खाना बनाने से जुड़ा बहुत ज़रूरी उत्पाद है। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल पाबंदी पर अब छूट दे दी है। लेकिन इसी तरह की पाबंदियां और जगह भी देखी गईं। हाल में मध्य एशिया के देशों से गेहूं उत्पादों के निर्यात पर पाबंदी लगाई गई। मलेशिया ने सिंगापुर को चिकन का निर्यात बंद कर दिया।
ये तमाम कदम खाद्य सुरक्षा के लिए उठाए गए। इनके साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी होती हैं।
डेविड लैबोर्ड कहते हैं, "पहली बात है उपलब्धता। क्या आपके पास खाने पीने का सामान मौजूद है? मात्रा भी मायने रखती है कि आपके पास कितना अनाज है? सामान तक पहुंच भी मायने रखती है कि क्या आपके पास खाने का सामान खरीदने के लिए पैसे हैं?"
निर्यात पर पाबंदी लगाने से देश में खाने का सामान उपलब्ध रहता है। कीमतें भी काबू में रहती हैं। लेकिन ये सिर्फ सिद्धांत की बात है। हकीकत में हमेशा ऐसा ही हो, ये ज़रूरी नहीं।
डेविड बताते हैं कि इंडोनेशिया में पाम ऑयल निर्यात पर पाबंदी लगी तो कई कंपनियों ने उत्पादन घटा दिया। घरेलू बाज़ार में माल बेचने के बजाए वो पाबंदी हटने का इंतज़ार करने लगीं।
हमारे एक्सपर्ट की राय है कि कुछ जगहों पर 'एक्सपोर्ट बैन' राजनीतिक संतुलन साधने का ज़रिया हो सकता है।
डेविड लैबोर्ड कहते हैं, "ऐसा इसलिए है कि कोई भी देश निर्यात पर रोक नहीं लगाता। सरकार लगाती है और सरकार का अपना एजेंडा होता है। कभी कभी मध्यम या निम्न आय वाले देशों में सरकार का ध्यान शहरी आबादी को राहत देने पर होता है। भले ही इसके लिए उन्हें ग्रामीण आबादी के हितों की कुर्बानी देनी पड़े। आप शहरों में खाने पीने के सामान की कीमत कम रखना चाहते हैं। इसकी वजह से चाहे आपके किसानों को कम कमाई हो और आपके केंद्रीय बैंक को कम विदेशी मुद्रा हासिल हो। "
विदेशी मुद्रा भंडार कम होने से देश की मुद्रा में गिरावट आती है। दूसरे देशों से खाने पीने का सामान आयात करना और महंगा हो जाता है। निर्यात पर रोक लगाने से देश की छवि भी खराब हो सकती है।
डेविड कहते हैं कि ऐसे देश को ग़ैरभरोसमंद व्यापारिक साझेदार माना जा सकता है और कंपनियां आपके देश में निवेश नहीं करना चाहेंगी।
वो कहते हैं कि इराक़ और अल्जीरिया जैसे कुछ देश अपना सामान निर्यात करने से मिली रकम के जरिए आयात बिल चुकाते हैं और किसानों की मदद करते हैं। लेकिन जिन देशों के पास संसाधन नहीं हैं, वो ऐसा नहीं कर पाते।
डेविड लैबोर्ड कहते हैं, " लेबनान और ट्यूनीशिया जैसे देशों की अर्थव्यवस्था सर्विस सेक्टर पर टिकी है। कोरोना महामारी के पर्यटन पर हुए असर और राजनीतिक अस्थिरिता के कारण उनके पास ऐसे मौके नहीं हैं। युद्ध की वजह से अगर अब खाने के सामान पर कोई नई पाबंदी लगती है तो निर्यात बिल और ज़्यादा बढ़ सकता है। फिर भी हम वैश्विक स्तर पर किसी अकाल की बात नहीं कर रहे हैं। हम बढ़ती खाद्य असुरक्षा और भूख की बढ़ती समस्या की बात कर रहे हैं। "
वो कहते हैं कि इसका असर 50 करोड़ या एक अरब लोगों पर हो सकता है। अगर खाद की स्थिति नियंत्रंण में नहीं आई तो अगले साल भंडार में अनाज काफी कम हो सकता है। तब हम कमी की बात कर रहे होंगे।
कब तक रहेगा संकट?
अमेरिका की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर डैनियल मैक्सवेल कहते हैं, "हम सूखे का मुक़ाबला कर सकते हैं। हम कोविड से निपट सकते हैं। ये एक बार आने वाले संकट हैं। युद्ध हर चीज को कहीं ज़्यादा मुश्किल बना देता है।"
वो कहते हैं कि खाद्य संकट लंबे समय तक बना रह सकता है। कोविड 19 महामारी के असर और बढ़ती महंगाई की वजह से खाद्य सुरक्षा पर संकट बढ़ गया है। डैनियल बताते हैं कि कई देशों के सामने तमाम तरह के संकट हैं।
इथियोपिया, दक्षिणी सूडान और सोमालिया में संघर्ष चल रहा है। 2020 और 2021 में टिड्डियों की समस्या भी रही है। तब फसलें नष्ट हो गईं। जानवरों के चरने के लिए कुछ नहीं बचा। इससे डेयरी और मीट मार्केट प्रभावित हुए।
डैनियल मैक्सवेल कहते हैं, "खान पान के सामान की कीमत दुनिया भर में पहले से ही बढ़ी हुई हैं। ये स्थिति बहुत हद तक वैसी ही हैं जैसे हमने 2011 में देखा था। अगर आप 2011 को याद करें तो उस साल सोमालिया में अकाल पड़ा था। उत्तरी अफ़्रीका और मध्य पूर्व में शहरी इलाकों में ब्रेड की कीमतें बढ़ने की बड़ी वजहों में से एक थी अरब स्प्रिंग यानी अरब क्रांति। यूक्रेन पर हमले के पहले ही खाद्य असुरक्षा की स्थिति बन रही थी।"
दुनिया भर में खाने के सामान की कीमतों में पहले भी उछाल आया है लेकिन इस बार स्थिति अलग है।
डैनियल मैक्सवेल बताते हैं, "संयुक्त राष्ट्र की फूड एग्रीक्लचर ऑर्गनाइजेशन ने इसे फूड प्राइस इंडेक्स में दिखाया है। ये 1974, 2008 और 2011 के मुकाबले ऊंचे स्तर पर है। अगर आप 2011 का इंडेक्स देखें तो पाएंगे कि तब भी उछाल आया था लेकिन तब ये कम समय के लिए था। मुझे लगता है कि इस बार गारंटी नहीं दी जा सकती है कि ये थोड़े समय के लिए ही है। "
इस साल मई में वर्ल्ड बैंक ने पुष्टि की कि अगले डेढ़ साल के दौरान व्यापक खाद्य संकट से मुक़ाबले के नए प्रोजेक्ट को 12 अरब डॉलर की अतिरिक्त रकम मुहैया कराई जाएगी। ये कुल रकम बढ़कर 30 अरब डॉलर हो जाएगी। संसाधन ज़्यादातर अफ़्रीका, मध्य पूर्व, पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के लिए होंगे।
डैनियल मैक्सवेल कहते हैं, "कुछ मामलों में भूख की समस्या से राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बन जाती है। आम तौर पर हम मानते हैं कि राजनीतिक उठापटक या फिर संघर्ष की वजह से भुखमरी की दिक्कत पैदा हो रही है लेकिन कई बार खाद्य संकट भी राजनीतिक समस्या या फिर उठापटक की वजह बन सकता है।"
तो क्या यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर में खाने के सामान का संकट खड़ा हो गया है? हमारे एक्सपर्ट बताते हैं कि दुनिया में अनाज तो उपलब्ध है लेकिन उस तक पहुंच नहीं होना संकट की मुख्य वजह है।
महामारी, सप्लाई चेन की दिक्कतें और तेज़ी से बढ़ती कीमतों जैसे दूसरे कारणों ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले ही दुनिया भर में सप्लाई सिस्टम को बाधित कर दिया था।
निर्यात पर पाबंदी से भी कोई लाभ नहीं हुआ। युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन के बंदरगाहों की घेरेबंदी का उन देशों पर बुरा असर हुआ है जो वहां से निर्यात होने वाले सामान पर निर्भर हैं। इस युद्ध ने आग भले ही न लगाई हो लेकिन बरसों से धधक रहीं लपटों को हवा ज़रूर दे दी है।