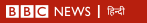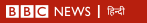रजनीश कुमार, बीबीसी संवाददाता
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पलट कर जवाब देने के मामले में अक्सर सुर्ख़ियों में रहते हैं। जयशंकर के इसी तेवर की आलोचना करते हुए सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा था कि इतनी पतली चमड़ी का होना ठीक नहीं है। थरूर ने कहा था कि जयशंकर को थोड़ा 'कूल' रहने की ज़रूरत है।
पश्चिम और पाकिस्तान को जवाब देने में जयशंकर कोई भी मौक़ा नहीं छोड़ते हैं, लेकिन चीन के मामले में उनका रुख़ बिल्कुल अलग होता है। चीन ने पिछले छह सालों में तीन बार अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों के नाम बदलकर मंदारिन में कर दिए हैं। चीन ने तीसरी बार इसी हफ़्ते सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम बदले हैं।
तीनों बार मोदी सरकार के रहते ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश में नाम बदले हैं। चीन के इस फ़ैसले का जवाब भारत के विदेश मंत्रालय ने बहुत ही सधी और सतर्क भाषा में दिया।
तिब्बत पर भारत को रुख़ बदलना चाहिए?
भारत ने अपने जवाब में कहा, ''हमने ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं। यह कोई पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह की कोशिश की है। हम इसे अस्वीकार करते हैं। अरुणाचल भारत का हिस्सा है, था और हमेशा रहेगा। इस तरह की कोशिश से हक़ीक़त नहीं बदल जाएगी।''
भारत के इस जवाब को कई विशेषज्ञ बहुत ही लचर और उदार मान रहे हैं। भारत के जाने-माने सामरिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने भारत के जवाब को रीट्वीट करते हुए लिखा है, ''चीन ने भारत को एक बार फिर से उकसाया है। एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों के नाम बदले हैं।''
''अरुणाचल प्रदेश ताइवान से लगभग तीन गुना ज़्यादा बड़ा है। एक बार फिर से भारत का विदेश मंत्रालय उचित जवाब देने में नाकाम रहा है। भारत का जवाब एक दिन के इंतज़ार के बाद बहुत ही नरमी वाला था।''
''सोशल मीडिया के ज़माने में समय पर जवाब देना मायने रखता है क्योंकि नैरेटिव सेट होने में बहुत वक़्त नहीं लगता है। चीन के सूचना युद्ध की तुलना में भारत सरकार अब भी धीमी है।''
अपने एक और ट्वीट में ब्रह्मा चेलानी ने लिखा है कि भारत इतना होने के बावजूद तिब्बत को चीन का अभिन्न हिस्सा मानता है। चेलानी ने लिखा है कि इससे ज़्यादा ख़ुद को नुक़सान पहुँचाने वाला और क्या हो सकता है?
ब्रह्मा चेलानी की बातों का समर्थन करते हुए भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने लिखा है, ''मैं इस बात से सहमत हूँ कि भारत का जवाब बहुत ही नरमी भरा है। भारत को और सख़्त भाषा में जवाब देना चाहिए था। अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना दावा तिब्बत को क़ब्ज़े में लेने के आधार पर करता है और ऐसे में हम भी अपने रुख़ में परिवर्तन ला सकते हैं।''
भारत का ढुलमुल रवैया?
क्या वाक़ई चीन की आक्रामकता के ख़िलाफ़ भारत का रवैया बहुत ही ढुलमुल है? ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन में स्टडी एंड फ़ॉरेन पॉलिसी के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफ़ेसर हर्ष वी पंत ऐसा नहीं मानते हैं।
प्रोफ़ेसर पंत कहते हैं, ''अरुणाचल को लेकर चीन जो कर रहा है, वह कोई नई बात नहीं है। भारत ने नाम बदलने को लेकर जो जवाब दिया है, वह पर्याप्त है। अरुणाचल में वैसी कोई दिक़्क़त भी नहीं है।''
''दिक़्क़त लद्दाख में है क्योंकि चीन वहाँ ज़मीन पर बहुत कुछ कर रहा है। भारत को वहाँ जवाब देना है। भारत वहाँ बोल कर जवाब नहीं दे सकता है। भारत भी बॉर्डर पर इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। चीन भी बोलता कम है और काम ज़्यादा कर रहा है। चीन का सामना बोलने से नहीं तैयारी करने से होगा।''
प्रोफ़ेसर पंत कहते हैं, ''अगर चार दशक पहले चीन को लेकर तैयारी हुई रहती तो भारत भी मुँहतोड़ जवाब देता। आपकी प्रतिक्रिया आपकी क्षमता पर निर्भर करती है। चीन 30 साल पहले जो प्रतिक्रिया देता था, वो आज नहीं है। उसकी क्षमता बढ़ी तो उसका जवाब भी आक्रामक हुआ।''
''भारत भी अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। आने वाले वक़्त में भारत का जवाब भी बदल सकता है। हमें चीज़ों को जटिल करने से कुछ हासिल नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि भारत तिब्बत को चीन का हिस्सा मानना बंद कर दे। वन चाइना पॉलिसी को मानने से इनकार कर दे। ऐसा तो अमेरिका भी नहीं कर पा रहा है तो हम ये सब करके क्या हासिल कर लेंगे?''
प्रोफ़ेसर पंत कहते हैं, ''अब तो दलाई लामा भी स्वतंत्र तिब्बत के बदले स्वायत्त तिब्बत की बात करते हैं। ताइवान में भी चीन को लेकर लोग बँटे हुए हैं। ऐसे में हम वन चाइना पॉलिसी को न मानकर क्या हासिल कर लेंगे?''
''हमने अतीत में बहुत ग़लतियां की हैं। चीन की आक्रामकता के सबूत लगातार मिल रहे थे, लेकिन हमने अपनी नीति नहीं बदली। अगर पहले ध्यान दिया होता तो स्थिति कुछ और होती।''
मोदी सरकार की नरमी के मायने
पिछले एक दशक में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चीन एक बड़ी चुनौती बन कर उभरा है। तीन साल पहले पूर्वी लद्दाख के गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हिंसक झड़प हुई थी। इसमें दोनों देशों के कुल 24 सैनिक मारे गए थे। तनाव अब भी क़ायम है और कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कहना है कि उसने चीन का सामना करने के लिए बॉर्डर पर भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती की है और सैन्य निर्माण के काम भी चल रहे हैं। कई ऐसी रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत ने 2020 में सीमा पर झड़प के बाद चीन के हाथों अपनी ज़मीन खोई है।
भारत के प्रधानमंत्री चीन को लेकर बोलने से बचते रहे हैं। मोदी सरकार की चुप्पी चीन के ख़िलाफ़ रणनीति का हिस्सा है या मजबूरी है?
नई दिल्ली स्थिति जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फ़ॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में असोसिएट प्रोफ़ेसर हैपीमोन जैकब ने अमेरिकी पत्रिका फ़ॉरेन पॉलिसी में दो अप्रैल को एक लेख लिखा है।
इस लेख में जैकब लिखते हैं, ''भारत की ओर से चीनी आक्रामकता को जवाब देना महज़ एक सैन्य सवाल नहीं है। यह राजनीतिक और कारोबारी हितों के कारण काफ़ी जटिल हो जाता है। ऐसे में भारत के लिए यह सोचना बहुत अहम हो जाता है कि अगर भारत चीन को जवाब देने का फ़ैसला करता है, तो कब और कैसे देगा।''
2022 में चीन का जीडीपी 18 ट्रिलियन डॉलर के क़रीब था और भारत का 3।5 ट्रिलियन डॉलर से भी कम था।
पिछले साल चीन का रक्षा बजट 230 अरब डॉलर था, जो भारत के रक्षा बजट से तीन गुना ज़्यादा था। चीन और भारत के बीच का यह अंतर ही भारत पर चीन को बढ़त दिलाता है।
हैपीमोन जैकब ने फ़ॉरेन पॉलिसी में लिखा है, ''अभी तक स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका या अन्य बड़ी शक्तियों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी क्या इस हद तक है कि चीन से टकराव की स्थिति में भारत के पक्ष में खुलकर आएगी या नहीं। भारत को कोई आश्वासन नहीं मिला है कि चीन से तनाव की स्थिति में उसके साझेदार खुलकर सामने आएँगे।''
''चीन पर भारत की कारोबारी निर्भरता है और दुनिया के किसी भी देश से भारत का कोई पारस्परिक डिफेंस क़रार नहीं है। सैन्य संकट के दौरान भारत समेत जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की सदस्यता वाले गुट क्वॉड की सैन्य मदद की कल्पना करना जल्दबाज़ी होगी। चीन से टकराव की स्थिति में बाहर के किसी देश से सैन्य मदद की उम्मीद अभी मुश्किल है।''
हैपीमोन जैकब ने लिखा है, ''भारत के पास कोई स्पष्ट योजना नहीं है कि वह चीन के साथ संघर्ष की स्थिति में पिछड़ गया, तो क्या करेगा। भारत से ज़्यादा ताक़त चीन के पास है और वह भारत के लिए एक द्वंद्व पैदा कर रहा है। भारत जीत के आश्वासन के साथ युद्ध में नहीं जा सकता और बिना हार के युद्ध की आशंका कम नहीं हो सकती। भारत छह दशक पहले चीन के साथ एक बड़ी हार देख चुका है।''
जैकब का कहना है कि चीन भारत को आर्थिक रूप से भी कई तरह की गंभीर चोट पहुँचा सकता है।
उन्होंने लिखा है, ''भारत दुनिया की पाँचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, तो इसमें चीन के सस्ते उत्पादों का भी योगदान है। ये उत्पाद उर्वरक से लेकर डेटा प्रोसेसिंग यूनिट तक हैं। सरहद पर चीन की आक्रामकता के ख़िलाफ़ उस पर व्यापारिक पाबंदी लगाना भारत पर ही भारी पड़ सकता है। हाल ही में अरविंद पनगढ़िया ने भी इसे रेखांकित किया था।''
तिब्बत पर किसकी ग़लती, नेहरू या वाजपेयी की?
2017 में भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह ने कहा था कि भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानकर बड़ी भूल की थी। बीजेपी के नाराज़ नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी आए दिन तिब्बत पर नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी को घेरते रहते हैं। क्या भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानकर वाक़ई ग़लती थी?
प्रोफ़ेसर हर्ष पंत कहते हैं, ''अतीत में हमने चीन को समझने में भूल तो की है। इन भूलों का नतीजा हम सबके सामने है। चीन को समझने में हमने देरी कर दी है।'' 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना था और चीन ने सिक्किम को भारत का हिस्सा।
आरसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइज़र के पूर्व संपादक शेषाद्री चारी ने बीबीसी से 2017 में कहा था, ''हमारी वो रणनीतिक भूल थी और हमने बहुत जल्दबाज़ी में ऐसा किया था। हमें तिब्बत को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए था। शुरू से हमें एक स्टैंड पर क़ायम रहना चाहिए था। हमें बिल्कुल साफ़ कहना चाहिए था कि चीन ने तिब्बत पर अवैध क़ब्ज़ा कर रखा है और यह स्वीकार नहीं है।''
चारी ने कहा था, "वाजेपयी सरकार को रणनीतिक तौर पर इसे टालना चाहिए था। उस वक़्त हमने तिब्बत के बदले सिक्किम को सेट किया था। चीन ने सिक्किम को मान्यता नहीं दी थी, लेकिन जब हमने तिब्बत को उसका हिस्सा माना तो उसने भी सिक्किम को भारत का हिस्सा मान लिया।"
चारी का कहना था, "इसके बाद ही नाथूला में सरहद पर ट्रेड को मंजूरी दी गई। नाथूला से इतना बड़ा व्यापार नहीं होता है कि इतनी बड़ी क़ीमत चुकानी चाहिए थी। तब ऐसा लगता था कि यह एक अस्थायी फ़ैसला है और बाद में स्थिति बदलेगी। उस वक़्त भारत ने दलाई लामा से भी बात की थी और उन्होंने इसकी मंज़ूरी भी दी थी।"
जेएनयू में सेंटर फ़ॉर चाइनीज़ एंड साउथ इस्ट एशिया स्टडीज़ के प्रोफ़ेसर बीआर दीपक का मानना है, "तिब्बत के मामले में भारत की बड़ी लचर नीति रही है। साल 1914 में शिमला समझौते के तहत मैकमोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा माना गया, लेकिन 1954 में नेहरू ने तिब्बत को एक समझौते के तहत चीन का हिस्सा मान लिया।"
प्रोफ़ेसर बीआर दीपक कहते हैं, "वाजपेयी और नेहरू में फ़र्क था। नेहरू ने आठ साल के लिए तिब्बत को चीन का हिस्सा माना था, लेकिन वाजपेयी ने कोई समय सीमा तय नहीं की थी।"
वह कहते हैं, "मार्च 1962 में नेहरू का चीन के साथ तिब्बत पर क़रार ख़त्म हो गया था और यह 2003 तक यथास्थिति रही। 2003 में जब वाजपेयी चीन के दौरे पर गए, तो उन्होंने तिब्बत पर समझौता कर कर लिया। भारत की नीति चीन और तिब्बत पर विरोधाभासों से भरी रही है। एक तरफ़ भारत मैकमोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा मानता है और तिब्बत को चीन का हिस्सा। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं। भारत का तिब्बत पर रुख़ एक जैसा होता, तो वह ज़्यादा अच्छा होता।''
बीआर दीपक मानते हैं कि भारत तिब्बत के मामले में अपना रुख़ बदल भी सकता है। जैसे पीएम मोदी अब दलाई लामा को जन्मदिन पर बधाई देते हैं और उन्हें अरुणाचल प्रदेश भी जाने की इजाज़त रहती है।
भारतीय इलाक़ों में चीनी अतिक्रमण की शुरुआत चीन ने 1950 के दशक के मध्य में शुरू कर दी थी।
1957 में चीन ने अक्साई चिन के रास्ते पश्चिम में 179 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई। इसी साल 21 अक्तूबर को लद्दाख के कोंगका में गोलीबारी हुई। इसमें 17 भारतीय सैनिकों की मौत हुई थी और चीन ने इसे आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया था।
कहा जाता है कि 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया तो ये केवल हिमालय के किसी इलाक़े पर नियंत्रण या सरहद को बदलने के लिए नहीं था बल्कि ये सभ्यता की जंग थी।