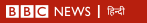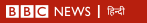- पुष्पेश पंत (फूड एक्सपर्ट)
दिल्ली के आसपास के इलाक़े की पुरानी कहावत है- माँस बिना सब घास रसोई! इस घड़ी जब देश की सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश में कसाईखाने ताबड़तोड़ युद्ध स्तर पर बंद कराए जा रहे हैं, हम कुछ घबराए यह सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि आने वाले दिन घास-फूस की जुगाली करते ही बिताने पड़ सकते हैं।
भारत में मांसाहार के बारे में प्रचलित मिथकों की वजह से कसाईखानों की तालाबंदी के बारे में ठंडे दिमाग से बहस करना लगभग असंभव हो गया है। ज़्यादातर लोग यह मानने को तैयार नहीं कि हिंदुस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा शुद्ध शाकाहारी नहीं है। जैन, कुछ ब्राह्मण और वैश्य ही इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं। कश्मीर के तथा मिथिला के ब्राह्मणों के पारंपरिक भोजन में शामिल व्यंजनों की लंबी सूची है। सागर तटवर्ती प्रदेश के निवासी सारस्वत ब्राह्मण तथा ओड़िया ब्राह्मण भी चाव से मांसाहार करते हैं।
माँस के गुण-दोष
कट्टर वैष्णवों के अलावा बंगाल और असम के शक्ति के उपासक माँस को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। राजस्थान में 'शूले' दहकते अंगारों पर भुने सींक कबाब की याद दिलाते हैं और 'खड ख़रगोश' अवधी जमींदोज मछली का रिश्तेदार लगता है। नाम भले 'शामी' न हो, संस्कृत की पुस्तकों में जिस मसालेदार 'भद्रितक' का जिक्र मिलता है वह गोलाकार टिकिया की शक्ल में माँसाहारी कबाब ही थे। माँस और मसालों के साथ घी में तले चावलों के 'पुलाव' से भी हिंदुस्तानी परिचित थे।।
तंदूरी मुर्ग़
पारसी रसोई में विभिन्न देशी-विदेशी पाक शैलियों का अनोखा संगम देखने को मिलता है। साली बोटी, धानसाक, जड़दालू गोश्त इसकी मिसाल हैं।
पंजाब फख़्र करता है तंदूरी मुर्ग़ की ईजाद पर तो साग गोश्त के चाहने वाले जात धर्म के आधार पर बाँटे नहीं जा सकते। यह बात दोहराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि इससे यह नतीजा निकालने की जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए कि हमारे देश में सभी लोग हमेशा गोश्त ही खाते रहते थे। हाँ, साधन संपन्न वर्ग की पौष्टिक स्वादिष्ट खुराक का हिस्सा माँस-मछली सदा से रहे हैं।
ईसा के जन्म से कई सौ साल पहले सोलह महाजनपदों के काल में जब बुद्ध उपदेश दे रहे थे और हिंसक वैदिक कर्म कांड को त्याग जनसाधारण उनकी ओर खिंच रहा था तब भी मठों में रहने वाले भिक्षु ही शाकाहारी थे। आबादी का बड़ा हिस्सा चाव से माँस खाता था।
महाभारत
स्वयं बुद्ध का देहांत भिक्षा पात्र में मिले दूषित मांस के कारण हुआ था, ऐसा माना जाता है। जातक कथाओं में राजपरिवारों एवं अमीर व्यापारियों के घरों का जो बखान मिलता है उससे यही बात पता चलती है। अहिंसा का संकल्प लेने के बाद भी सम्राट अशोक के महल में परंपरा के निर्वाह के लिए माँस पकता था इसका जिक्र उनके शिलालेखों में दर्ज है।
महाभारत का रचनाकाल चौथी सदी ईस्वी पूर्व से चौथी सदी ईस्वी के बीच माना जाता है। इसमें भारत वर्ष के अनेक प्रदेशों के निवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी की झलकियों के साथ-साथ त्योहारों, शादी ब्याह के मौक़ों पर पकाए, खाए जाने वाले पकवानों का जो वर्णन मिलता है उससे भी यही साबित होता है कि देश भर में माँस खाया जाता था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के वक़्त जो राजा महाराजा इंद्रप्रस्थ पहुँचे उनकी ख़ातिरदारी में पेश माँस की कई किस्म के व्यंजनों का बखान सुलभ है।
शाकाहार या मांसाहार
दिलचस्प बात यह है कि कई जगह ब्राह्मण मेहमानों के लिए तैयार किए जाने वाला भोजन भी पूर्णत: शाकाहारी नहीं होता था। क्षत्रिय शासक ही नहीं, वनवासी आदिवासी भी माँसाहारी रहे हैं। राजसिक और तामसिक मिज़ाज के व्यक्ति अपने स्वभाव और प्रकृति के मुताबिक़ इच्छानुसार शाकाहार या मांसाहार करने को स्वतंत्र थे।
जिन सात्विक लोगों के लिए माँस वर्जित समझा जाता था वह भी दूसरे आहार के अभाव में आपत्धर्म के अनुसार माँस खा सकते थे। ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार यह घोषणा जायज़ नहीं कि गोश्तखोरी को किसी मज़हब या संप्रदाय विशेष के साथ जोड़ा जा सकता है।
हैदराबाद की बिरयानी
यह ज़रूर सच है कि बहुसंख्यक आबादी के लिए वर्जित गोमांस खाने से परहेज़ न करने वाले मुसलमानों और बाद में अंग्रेज (अन्य यूरोपीय) ईसाइयों के आगमन के बाद ही मांसाहार को 'फिरंगी विधर्मियों' के साथ जोड़कर दूषित समझने वाली मानसिकता प्रबल हुई। हिंदुस्तान के अलग-अलग प्रदेशों के निवासी अपनी सांस्कृतिक विरासत में अपने खान-पान को प्रमुख स्थान देते आए हैं।
कश्मीर में वाजवान की दो धाराएँ देखने को मिलती हैं। पंडित वाजवान माँसाहारी व्यंजनों में मुसलमान वाजवान से होड़ लेता है। अवध के गलौटी काकोरी कबाब, दम पुख्त, दिल्ली का इष्टू और पसंदे और हैदराबाद की बिरयानी, हलीम और दाल्चा गोश्त इन जगहों की देखने लायक इमारतों या संगीत और साहित्य से कम दिलकश नहीं। स्थानीय पहचान इन व्यंजनों के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी है। फिर एक बार सतर्क रहने की ज़रूरत है।
माँसाहारी खाना सिर्फ़ तुर्कों- अफ़ग़ानों और मुग़लों की देन नहीं। आज से हज़ार साल पहले चोल सम्राट दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुँच चुके थे। उस वक़्त के चेट्टियार नाविक सौदागर शौक से कई क़िस्म के सूखे और तरीवाले माँसाहारी व्यंजन खाते थे। वास्तव में अंग्रेज़ी का 'करी' शब्द तमिल 'कारी' का ही अपभ्रंश है।
तमिलनाडु के सौदागर दो हज़ार साल पहले रोम के साथ व्यापार कर रहे थे और मलाबार तट अरब जगत से आने वाले व्यापारियों के संपर्क में रहा है। यह सोचना तर्क संगत नहीं कि यह आदान-प्रदान शुद्ध शाकाहारी रहा है!
(यह लेखक के निजी विचार हैं।)