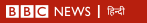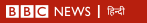- रेहान फ़ज़ल
"साढ़े पाँच फ़ुट का क़द, जो किसी तरह सीधा किया जा सके तो छह फ़ुट का हो जाए, लंबी-लंबी लचकीली टाँगें, पतली सी कमर, चौड़ा सीना, चेहरे पर चेचक के दाग़, सरकश नाक, ख़ूबसूरत आँखें, आंखों से झींपा -झींपा सा तफ़क्कुर, बड़े-बड़े बाल, जिस्म पर क़मीज़, मुड़ी हुई पतलून और हाथ में सिगरेट का टिन।" ये थे साहिर लुधियानवी, उनके दोस्त और शायर कैफ़ी आज़मी की नज़र में।
साहिर को क़रीब से जानने वाले उनके एक और दोस्त प्रकाश पंडित उनकी झलक कुछ इस तरीक़े से देते हैं, "साहिर अभी-अभी सो कर उठा है (प्राय: 10-11 बजे से पहले वो कभी सो कर नहीं उठता) और नियमानुसार अपने लंबे क़द की जलेबी बनाए, लंबे-लंबे पीछे को पलटने वाले बाल बिखराए, बड़ी-बड़ी आँखों से किसी बिंदु पर टिकटिकी बाँधे बैठा है (इस समय अपनी इस समाधि में वो किसी तरह का विघ्न सहन नहीं कर सकता... यहाँ तक कि अपनी प्यारी माँजी का भी नहीं, जिनका वो बहुत आदर करता है) कि यकायक साहिर पर एक दौरा-सा पड़ता है और वो चिल्लाता है- चाय!"
"और सुबह की इस आवाज़ के बाद दिन भर, और मौक़ा मिले तो रात भर, वो निरंतर बोले चला जाता है। मित्रों- परिचितों का जमघटा उस के लिए दैवी वरदान से कम नहीं। उन्हें वो सिगरेट पर सिगरेट पेश करता है (गला अधिक ख़राब न हो इसलिए ख़ुद सिगरेट के दो टुकड़े करके पीता है, लेकिन अक्सर दोनों टुकड़े एक साथ पी जाता है।) चाय के प्याले के प्याले उनके कंठ में उंडेलता है और इस बीच अपनी नज़्मों-ग़ज़लों के अलावा दर्जनों दूसरे शायरों के सैकड़ों शेर, दिलचस्प भूमिका के साथ सुनाता चला जाता है।"
सुनें विवेचनाःनर्म लहज़े का शायर साहिर
एक बार पंजाब के एक शायर नरेश कुमार शाद को साहिर लुधियानवी का इंटरव्यू लेने का मौक़ा मिला। जैसा कि रिवाज होता है उन्होंने पहला सवाल दाग़ा, "आपकी पैदाइश कहाँ और कब हुई?"
साहिर की पैदाइश
साहिर ने जवाब दिया, "ऐ जिद्दत पसंद नौजवान, ये तो बड़ा रवायती सवाल है। इस रवायत को आगे बढ़ाते हुए इसमें इतना इज़ाफ़ा और कर लो- क्यों पैदा हुए?"
विभाजन के बाद साहिर पाकिस्तान चले गए। नामी फ़िल्म निर्देशक और उपन्यासकार ख़्वाजा अहमद अब्बास ने उनके नाम 'इंडिया वीकली' पत्रिका में एक खुला पत्र लिखा। अब्बास अपनी आत्मकथा 'आई एम नॉट एन आइलैंड' में लिखते हैं, "मैंने साहिर से अपील की कि तुम वापस भारत लौट आओ। मैंने उन्हें याद दिलाया कि जब तक तुम अपना नाम नहीं बदलते, तुम भारतीय शायर ही कहलाओगे। हाँ, ये बात अलग है कि पाकिस्तान भारत पर हमला कर लुधियाना पर क़ब्ज़ा कर ले।"
"मुझे ख़ासा आश्चर्य हुआ जब इस पत्रिका की कुछ प्रतियाँ लाहौर पहुंच गईं और साहिर ने मेरा पत्र पढ़ा। मेरी ख़ुशी का ठिकाना नहीं रहा जब साहिर ने मेरी बात मानी और अपनी बूढ़ी माँ के साथ भारत वापस आ गए और न सिर्फ़ उर्दू अदब बल्कि फ़िल्मी दुनिया में काफ़ी नाम कमाया।"
जब साहिर की ग़ज़ल 'ताजमहल' प्रकाशित हुई तो हर ख़ास-ओ-आम की ज़बाँ पर चढ़ गई। तारीफ़ के साथ-साथ कुछ दक्षिणपंथी उर्दू अख़बारों ने साहिर की ये कह कर आलोचना की कि उन जैसे एक नास्तिक शख़्स ने बिना वजह महान सम्राट शाहजहाँ की बेइज़्जती की है। ग़ज़ल का एक शेर था-
ताजमहल पर साहिर
दिलचस्प बात ये है कि इसे लिखने से पहले साहिर न तो कभी आगरा गए थे और न ही उन्होंने ताजमहल देखा था। अपने एक दोस्त साबिर दत्त को इसकी सफ़ाई देते हुए साहिर ने कहा था, "इसके लिए मुझे आगरा जाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने मार्क्स का फ़लसफ़ा पढ़ा हुआ था। मुझे मेरा भूगोल भी याद था। ये भी पता था कि ताजमहल जमुना के किनारे शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए बनवाया था।"
साहिर से जुड़ा एक दिलचस्प क़िस्सा स्टार पब्लिकेशंस के प्रमुख अमर वर्मा सुनाते हैं जो उनके दोस्त भी थे और प्रकाशक भी। वो बताते हैं, "मेरी उनसे पहली मुलाक़ात 1957 में दिल्ली में हुई थी। मैंने स्टार पॉकेट बुक्स में एक रुपये क़ीमत में एक सिरीज़ शुरू की थी। मैं चाहता था कि उसकी पहली किताब साहिर साहब की हो। मैंने कहा कि मैं आपकी किताब छापने की इजाज़त चाहता हूँ। वो बोले मेरी तल्ख़ियाँ क़रीब-क़रीब दिल्ली के हर प्रकाशक ने छाप दी है बिना मेरी इजाज़त लिए हुए। आप भी छाप दीजिए। जब मैंने ज़ोर दिया तो उन्होंने कहा कि आप मेरे फ़िल्मी गीतों का मजमुआ छाप दीजिए, गाता जाए बनजारा के नाम से।"
"न भूलने वाली बात ये है कि कुछ वक़्त बाद मैंने उन्हें बहुत झिझकते हुए रॉयल्टी का 62 रुपए 50 पैसे का चेक भेजा। तय हुआ था कि मैं उनकी किताब की हज़ार प्रतियाँ छापूँगा और सवा छह फ़ीसदी की रॉयल्टी दूँगा। साहिर को इतनी छोटी रक़म भेजते हुए मैं डर रहा था कि वो पता नहीं क्या सोचेंगे। साहिर का मेरे पास जवाब आया...आप इसे मामूली रक़म मानते हैं। ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मुझे रॉयल्टी दी है। इस चेक को तो मैं ज़िंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा।" इतने बड़े शायर होने के बावजूद ज़रा-सी बात पर उकता जाना, घबरा जाना या शरमा जाना साहिर का स्वभाव था।
शर्मीले साहिर
उन पर किताब लिखने वाले अक्षय मनवानी बताते हैं कि एक ज़माने में छात्र नेता रहे साहिर लुधियानवी बड़े जमघट को देखकर कभी उत्साहित नहीं होते थे। "माइक्रोफ़ोन के नज़दीक जाते ही उनकी ज़ुबान जैसे सिल जाती थी। सुनने वालों का एक वर्ग फ़रमाइश करता था कि वो ताजमहल सुनाएं, तो दूसरी तरफ़ से फ़नकार सुनाने की आवाज़ आती थी। दोनों फ़रमाइशों के बीच वो अक्सर भूल जाते थे कि उन्होंने वहाँ सुनाने के लिए कौन सी नज़्म चुनी है।"
ये अनिर्णय की स्थिति इस हद तक पहुंचती थी कि साहिर की समझ में नहीं आता था कि मुशायरे के वक़्त वो कौन-से कपड़े पहनें। यहाँ तक कि किस क़मीज़ पर वो कौन-सी पतलून पहनें, इसके लिए उन्हें अपने दोस्तों की मदद लेनी पड़ती थी। उनके दोस्त प्रकाश पंडित लिखते हैं, "उनके दोस्त तय करते थे कि वो नाश्ते में पराठे आमलेट खाएं या टोस्ट मक्खन। साहिर की इन्हीं आदतों के कारण कभी-कभी हम दोनों में ठन भी जाती थी। जब वो लिबास के बारे में मेरी राय लेता तो मैं बड़ी गंभीरता से कपड़े छाँटकर उसे अच्छा ख़ासा कार्टून बना देता और नाश्ता तो मैंने उसे कई बार आइसक्रीम तक का करवाया। लेकिन धीरे-धीरे मुझे लगने लगा कि वो मज़ाक़ नहीं दया का पात्र है। ये आदतें उसने ख़ुद नहीं पालीं। इसकी तह में काम करती थीं वो परिस्थितियाँ, जिनमें उसने आँखें खोलीं, परवान चढ़ा और जो अपने समस्त गुणों-अवगुणों के साथ उसके व्यक्तित्व का अंग बन गईं।"
अमृता प्रीतम से नाता
बंबई के उनके शुरू के दिनों में जब उन्हें कोई काम नहीं मिला तो उनके दोस्त मोहन सहगल ने उन्हें बताया कि मशहूर संगीतकार एसडी बर्मन एक गीतकार की तलाश में हैं। उस समय बर्मन ने खार में ग्रीन होटल में एक कमरा ले रखा था। उसके बाहर 'प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब' का साइन लगा हुआ था।
इसके बावजूद साहिर सीधे बर्मन के कमरे में घुस गए और अपना परिचय कराया। एसडी बर्मन चूँकि बंगाली थे, इसलिए उर्दू साहित्य में साहिर के क़द के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने साहिर को एक धुन दी। फ़िल्म की सिचुएशन समझाई और एक गीत लिखने के लिए दिया। साहिर ने बर्मन से वो धुन एक बार फिर से सुनाने के लिए कहा। जैसे ही बर्मन ने उसे हारमोनियम पर बजाना शुरू किया साहिर ने लिखा, "ठंडी हवाएं, लहरा के आएं, रुत है जवाँ, तुम हो यहाँ, कैसे भुलाएं।"
लता मंगेशकर के गाए इस गीत ने बर्मन-साहिर जोड़ी की नींव रखी जो कई सालों तक चली। गुरुदत्त की फ़िल्म 'प्यासा' के गीत और संगीत दोनों ने उस समय पूरे भारत में खलबली मचा दी। भारतीय फ़िल्म इतिहास का सबसे काव्यात्मक क्षण तब आया जब गुरुदत्त ने साहिर की नज़्म गुनगुनाई, 'ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है।'
फ़िल्म इंडस्ट्री में हमेशा से ही संगीतकारों को गीतकारों की तुलना में ज़्यादा अहमियत मिलती आई है। बर्मन और साहिर दोनों का मानना था कि 'प्यासा' की सफलता के वो हक़दार हैं। साहिर का ज़ोर-शोर से ये कहना एसडी बर्मन को पसंद नहीं आया और उन्होंने साहिर के साथ दोबारा काम करने से इंकार कर दिया।
साहिर का नाम कई महिलाओं के साथ जुड़ा लेकिन उन्होंने ताउम्र शादी नहीं की। उनकी सबसे नज़दीकी दोस्त थीं अमृता प्रीतम। वो अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में लिखती हैं, "वो चुपचाप मेरे कमरे में सिगरेट पिया करता। आधी पीने के बाद सिगरेट बुझा देता और नई सिगरेट सुलगा लेता। जब वो जाता तो कमरे में उसकी पी हुई सिगरेटों की महक बची रहती। मैं उन सिगरेट के बटों को संभाल कर रखतीं और अकेले में उन बटों को दोबारा सुलगाती। जब मैं उन्हें अपनी उंगलियों में पकड़ती तो मुझे लगता कि मैं साहिर के हाथों को छू रही हूँ। इस तरह मुझे सिगरेट पीने की लत लगी।"
सुधा मल्होत्रा
पार्श्व गायिका सुधा मल्होत्रा का नाम भी साहिर के साथ जोड़ा गया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये साहिर का एकतरफ़ा प्यार था। अक्षय मनवानी कहते हैं, "सुधा ने मुझे बताया...शायद साहिर को मेरी आवाज़ अच्छी लगती थी। वो मुझसे मोहित ज़रूर थे। उन्होंने मुझे गाने के लिए लगातार अच्छे गाने दिए। रोज़ सुबह मेरे पास उनका फ़ोन आता था। मेरे चाचा मुझे चिढ़ाया करते थे...तेरे मॉर्निंग अलार्म का फ़ोन आ गया। लेकिन ये ग़लत है कि मेरा उनसे कोई रोमांस चल रहा था। वो मुझसे उम्र में कहीं बड़े थे।"
लेकिन कहा ये जाता था कि फ़िल्म गुमराह में साहिर का लिखा महेंद्र कपूर का गाया गाना 'चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं' वास्तव में सुधा मल्होत्रा के लिए लिखा गया था। लेकिन सच बात ये थी कि ये नज़्म साहिर की सुधा से मुलाक़ात से कहीं पहले उनके काव्य संग्रह तल्ख़ियाँ में ख़ूबसूरत मोड़ के नाम से प्रकाशित हो चुकी थीं।
1960 में अपनी शादी के बाद सुधा ने हिंदी फ़िल्मों के लिए कोई गाना नहीं गाया। उनकी साहिर से फिर कभी मुलाक़ात भी नहीं हुई। साहिर का लिखा एक गीत जिसे सुधा मल्होत्रा ने गाया, उन दोनों के संबंधों को शायद सही ढंग से रेखांकित करता है-
लिफ़्ट में डर
साहिर को लिफ़्ट इस्तेमाल करने से डर लगता था। जब भी यश चोपड़ा उन्हें किसी संगीतकार के साथ काम करने की सलाह देते तो वो उस संगीतकार की योग्यता उसके घर के पते से मापते थे..."अरे नहीं नहीं, वो ग्यारहवीं मंज़िल पर रहता है...जाने दीजिए छोड़िए।
इसको लीजिए...ये ग्राउंड फ़्लोर पर रहता है।" मज़े की बात है कि यश चोपड़ा साहिर की बात सुना करते थे। लिफ़्ट की तरह साहिर को जहाज़ पर उड़ने भी डर लगता था। वो हर जगह कार से जाते थे। उनके पीछे एक और कार चला करती थी कि कहीं जिस कार में वो सफ़र कर रहे हैं वो ख़राब न हो जाए।
एक बार वो कार से लुधियाना जा रहे थे। मशहूर उपन्यासकार कृशन चंदर भी उनके साथ थे। शिवपुरी के पास डाकू मान सिंह ने उनकी कार रोक कर उसमें सवार सभी लोगों को बंधक बना लिया। जब साहिर ने उन्हें बताया कि उन्होंने ही डाकुओं के जीवन पर बनी फ़िल्म 'मुझे जीने दो' के गाने लिखे थे तो उन्होंने उन्हें इज़्ज़त से जाने दिया था।